बौद्ध कालीन शिक्षा, दिनचर्या, अध्ययन पद्धति, प्रमुख केंद्र
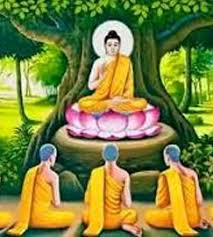
Table of Contents
बौद्ध कालीन शिक्षा (buddhist education system)
बौद्ध कालीन शिक्षा क्या है-(buddhist education system)
हिंदू धर्म में आए हुए दोषों के निराकरण के लिए बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ।
बुद्ध ने जनसाधारण के लिए एक सरल मार्ग बतलाया जिससे वह सांसारिक दुःखों से छुटकारा पा सके।
बौद्ध धर्म में सर्वसाधारण के लिए निर्वाण मार्ग का स्पष्टीकरण किया गया है।
तथा बौद्ध कालीन शिक्षा बौद्ध विहारों,संघों या मठों में दी जाती थी ।
तथा शिक्षा पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता था।
बौद्ध कालीन शिक्षा भी दो भागों में विभाजित थी प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा।
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी तथा उच्च शिक्षा के लिए शुल्क देना पड़ता था।
शिक्षा की शुरुआत प्रबज्जा (पबज्जा) संस्कार से होती थी जिसकी उम्र सबके लिए लगभग 6 वर्ष थी।
इसके बाद ही छात्रों को मठ में प्रवेश मिलता था तथा मठों में निवास करने वाले छात्रों को ‘सामनेर या श्रमण’कहा जाता था।
अध्यापक को उपाध्याय या उपाझियाय कहा जाता था।
प्राथमिक स्तर पर प्राकृत भाषा सिखाने के लिए “सिद्धहस्त बालपोथी” नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी,जिसमें 46 अक्षर होते थे।
बौद्ध धर्म का विकास संघों के रूप में हुआ। संघ ही बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
संघों के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं था,क्योंकि बौद्ध शिक्षा का संबंध पूर्णतः संघ से ही था।
बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत केवल संघ के श्रमणों को ही धार्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।
श्रमणों के अतिरिक्त अन्य लोगों को शिक्षा देने का अधिकार संघों को प्राप्त नहीं था।
वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति यज्ञ के अनुष्ठान में ही पल्लवित हुई थी,
बौद्ध काल में संघ ने यज्ञ का स्थान ले लिया।
अतः बौद्ध संघ की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति है।
संघ प्रवेश:-
संघ में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष नियम थे, जिनको हम ब्राह्मणी शिक्षा के अंतर्गत भी पाते हैं।
ब्रह्मचारियों की भांति ही बौद्ध भिक्षु को गुरु के सामने जाकर यह प्रार्थना करनी पड़ती थी, कि उसको शिष्य के रूप में ग्रहण करें।
बौद्ध संघों में शिष्य का संबंध गुरु से होता था, संघ के भिक्षु से नहीं।
गुरु पर ही भिक्षु विद्यार्थी का संपूर्ण उत्तरदायित्व रहता था संघ उसका उत्तरदाई नहीं होता था।
इस प्रकार गुरु शिष्य का व्यक्तिगत संबंध बौद्ध शिक्षा में भी पाया जाता है।
प्रबज्जा (पबज्जा):-
प्रबज्जा( पबज्जा) का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना।
भावी भिक्षु प्रथा के अनुसार अपने पारिवारिक संबंध से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था।
संघ में सभी वर्ग के लोग प्रवेश पाने के अधिकारी थे।
संघ में आ जाने के बाद उनका कोई वर्ण नहीं रह जाता था,
यहां तक कि उनका पहला चरित्र और पहले के वस्त्र भी बदल जाते थे।
अतः बौद्ध कालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है,
जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी।
किंतु साधारणतया उच्च वर्ग के लोग ही अधिकतर संघ में प्रवेश पाते थे।
भावी भिक्षु को प्रबज्जा ग्रहण करने के समय 8 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक संघ में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 20 वर्ष की आयु में वह “उपसंपदा संस्कार” ग्रहण करता था।
उप संपदा संस्कार के उपरांत वह संघ का पूर्णरूपेण सदस्य बन जाता था।
8 वर्ष की उम्र का भावी भिक्षु सिर मुड़ा कर पीला वस्त्र हाथ में लिए हुए स्वेच्छा से किसी मठ में जाकर तथा किसी प्रमुख भिक्षु के समक्ष उपस्थित होता था, और उसकी शरण में अपने को अर्पित करते हुए संघ में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना करता था।
भिक्षु उस भावी भिक्षु को पीला वस्त्र धारण करवाता तथा सरणत्तय (शरणत्रयि-तीन वादे): बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि तीन वर्णों का तीव्र ध्वनि से उच्चारण करवाता था।
इस प्रकार पबज्जा के उपरांत ही भिक्षुओं को “सामनेर” कहा जाता था।
तदुपरांत सामनेर को 10 आदेश दिए जाते थे जो निम्नलिखित थे।
1. जीव हिंसा ना करना।
2. अशुद्ध आचरण से दूर रहना।
3.असत्य भाषण ना करना।- 4. कुसमय में आहार ना करना ।
5. मादक वस्तुओं का उपयोग ना करना।
6. किसी की निंदा ना करना।
7. श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग ना करना।
8. नृत्य आदि तमाशों के निकट ना जाना।
9. बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ग्रहण ना करना।
10. सोना, चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों का दान ना लेना।
इन 10 आदेशों को “दश शिक्क्षा पदानि” कहते थे, और सामनेर अथवा श्रमण के लिए इनका पालन करना अनिवार्य था।
20 वर्ष की आयु तक श्रमण का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर रहता था।
यहां यह बात ध्यान देने की है कि
बालक का संघ में प्रवेश उसके माता-पिता की सहमति पर ही होता था,
तथा कोढ़, खुजली आदि संक्रामक रोग ग्रस्त भी संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे और दास, राज्य कर्मचारी तथा सैनिक आदि के लिए भी प्रवेश निषिद्ध था।
उपसंपदा संस्कार:-
उप संपदा के संपादन की विधि पबज्जा से भिन्न होती थी।
श्रमण 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा में संलग्न रहने के उपरांत 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर संघ के समस्त सदस्यों के समक्ष उपस्थित होता था।
उप संपदा के संपादन की प्रणाली जनतांत्रिक थी।
संघ के सदस्यों के नेता एक के अथवा बहुमत द्वारा कोई भी उपसंपदा ग्रहण करके समस्त जीवन के लिए संघ का स्थाई सदस्य बन जाता था।
उपसंपदा के बाद श्रमण पक्का भिक्षु बन जाता
और उसका गृहस्ती अथवा सांसारिक बंधनों से कोई संबंध नहीं रह जाता था।
बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य लेनदेन तथा बौद्ध धर्म के तीन ग्रंथों: सूत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का ज्ञान होना अनिवार्य था।
शिक्षा भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह लौकिक एवं पारलौकिक दो प्रकार की थी।
शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी,जो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा थी कहीं-कहीं पालि भाषा भी देखने को मिलती है।
बौद्ध कालीन गुरु का कर्तव्य:-
संघ पर गुरु शिष्य दोनों ही आश्रित थे।
संघ द्वारा गुरु के कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे।
शिष्य का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर होता था।
गुरु के लिए आवश्यक था कि वह शिष्य को पुत्र की भांति शिक्षा दें,
तथा दैनिक कार्यों के अंतर्गत शिष्य के भिक्षाटन के लिए यदि बर्तन की आवश्यकता हो तो उसका प्रबंध करें।
वस्त्र अथवा अन्य किसी वस्तु की कमी को भी गुरु को ही पूरा करना होता था।
शिष्य के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व भी गुरु पर था।
शिष्य के अस्वस्थ होने पर गुरु को उसकी पूरी परिचर्या करनी पड़ती थी
और जबतक वह बीमारी के पश्चात पूर्ण स्वस्थ ना हो जाए उसकी सेवा करता था।
मानसिक विकास के लिए गुरु व्याख्यान एवं प्रश्न उत्तर आदि नीतियों से शिष्य को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते थे।
बौद्ध कालीन छात्रों की दिनचर्या:-
छात्र नियमित रूप से अपने गुरु की सेवा करते थे।
गुरु सेवा शिक्षा का एक प्रमुख अंग थी। छात्र की दिनचर्या उसके अनेक कर्तव्यों से पूर्ण थी।
प्रातः काल उठकर वह गुरु के लिए आसन लगाते, दातुन रखते तथा हाथ मुंह धोने के लिए पानी का प्रबंध करते थे, इसके बाद भोजन तैयार करना भी शिष्य का कार्य था।
पहले गुरु को भोजन करवाते और फिर उनका बर्तन आदि धोना होता था।
गुरु के भिक्षाटन के लिए पात्र, वस्त्र आदि गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते और गुरु की आज्ञा होने पर उनके साथ भिक्षाटन के लिए भी जाते।
भिक्षाटन के लिए जाने पर शिष्य को आचार्य से पहले विहार में लौट आना पड़ता था और यहां आकर गुरु के हाथ पैर धोने वस्त्र बदलने तथा विश्राम के लिए प्रबंध करना होता था।
शिष्य आचार्य की इच्छा अनुकूल कुछ भोजन भी प्रस्तुत करता था।
अपने स्नान आदि से शीघ्र निवृत्त होकर वह गुरु के लिए शीतल अथवा गर्म जल की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करता तथा शरीर लेप के लिए मिट्टी आदि प्रस्तुत करता था।
आचार्य की इच्छा होने पर वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता और तत्कालीन सामान्य प्रचलित प्रणाली के अनुसार शिष्य गुरु से प्रश्न करता और गुरु उनके उत्तर में उपदेश देता था।
आचार्य की सेवा के अतिरिक्त आचार्य के निवास स्थान की सफाई, सामान को ठीक ढंग से रखना, भंडार तथा रसोई आदि की व्यवस्था करना भी शिष्य का कार्य था।
शिष्य पर गुरु की आज्ञा का पूर्ण अनुशासन था। गुरु की आज्ञा के बिना वह कहीं नहीं जा सकता था।
शिष्य किसी अन्य से सेवा भी नहीं करवा सकता था और ना किसी की आज्ञा ही उसके लिए मान्य थी।
निष्कासन:-
विहार से विद्यार्थी के अलग होने के लिए निश्चित अवस्थाएं थी।
गुरु को शिष्य के निष्कासन का अधिकार था।
जब वह अनुभव करता कि शिष्य में श्रद्धा, सम्मान तथा शिक्षा के प्रति भक्ति की कमी आ गई है, अथवा वह ऐसा कर सकने में सर्वदा समर्थ नहीं है तब गुरु शिष्य को अपने शिष्यत्व से अलग कर सकता था।
इसके अतिरिक्त अन्य अवस्था में जैसे शिक्षक की मृत्यु हो जाने पर उसके अन्य धर्म को स्वीकार कर लेने पर संघ से बाहर चले जाने पर तथा गृहस्त हो जाने पर शिष्य की शिक्षा संभवत समाप्त समझी जाती थी
और उसको संघ से अलग हो जाना होता था।
छात्रों की संख्या तथा निवास स्थान:-
बौद्ध शिक्षा में एक भिक्षु एक भावी भिक्षु की शिक्षा के संपादन का कार्य ग्रहण करता था। किंतु समर्थ शिक्षकों को अधिक शिष्यों को भी शिक्षा देने की अनुमति बुद्ध ने प्रदान की थी।
बौद्ध विहार मठों के द्वारा ही संघ बनते थे। मठों में विद्यार्थी और आचार्य एक साथ निवास करते थे।
साधारणतया अनुकूल मौसमों में बौद्ध भिक्षु पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहते थे किंतु वर्षा ऋतु में आंधी तीव्र धूप होने पर उनको मठों और विहारों में रहने की आज्ञा थी।
इन विहारों और मठों के विशाल भवनों का निर्माण सम्राटों अथवा धनीक लोगों द्वारा होता था। किसी किसी विहार के प्रासाद में सहस्त्रों विद्यार्थियों के निवास की व्यवस्था थी।
नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष इस कथन की पुष्टि करते हैं।
विहारों में शयन, भोजन, स्नान, अध्ययन, वाचन, शास्त्रार्थ तथा अतिथि सम्मान के लिए अलग-अलग कमरे बने होते थे।
राजकुमार अनाथ पंडित द्वारा निर्मित तेतवन विहार में इसी प्रकार की व्यवस्था थी।
इन विहारों का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए होता था, वरन यह उस समय बौद्ध शिक्षा के केंद्र भी थे, जहां कला कौशल आदि भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी।
विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावासों का भी वर्णन मिलता है।
बौद्ध कालीन अध्ययन पद्धति:-
बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था।
वैयक्तिक विकास में मानसिक तथा नैतिक स्तर का उच्च होना स्वभाविक था और पूर्ण वैयक्तिक विकास के बिना बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त करना सर्वथा असंभव था।
प्रारंभिक शिक्षा में धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। संभवत प्रारंभ में छात्र सुनते रहते तथा एक दूसरे को सुनकर उनको कंठस्थ करते थे।
विनय की शिक्षा भी आवश्यक थी।
विनय के पश्चात उनको विभिन्न शैलियों के अंतर्गत धर्म के प्रशिक्षण द्वारा भविष्य के लिए समस्त धार्मिक विशेषताओं से परिचित कराया जाता था।
इसके लिए विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ वाद-विवाद करके धर्म संबंधी बातों की गहराई तक पहुंच कर, भविष्य में धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपने को तैयार करता था।
अजंता गुफा का चित्र नंबर 16 नीचे दिया जा रहा है इसके द्वारा यह पता चलता है कि उस समय शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार था और किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी।
शिक्षा में भिन्नता की थी। ऐसे भिक्षु का भी वर्णन मिलता है जो निर्जन में रहकर चिंतन मनन करके शिक्षा ग्रहण करते थे।
तपस्या और साधना के द्वारा उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करते थे।
इसके विपरीत ऐसे भी बिच्छू थे जिनमें सांसारिक प्रवृत्ति की प्रबलता थी, और वह भौतिक विषयों के ज्ञान और शारीरिक शक्ति पर अधिक ध्यान देते थे।
इन भिन्न-भिन्न भिक्षुओं का अलग-अलग निवास स्थान होता था जिससे एक दूसरे के अध्ययन में बाधा ना पड़े।
कुछ विभिन्न अध्ययन प्रणालियों का विवरण दिया जा रहा है।—
मौखिक:-
लेखन कला का प्रचार बौद्ध काल तक हो चुका था किंतु शिक्षा पद्धति में मौखिक प्रणाली पूर्णतः प्रचलित थी। हो सकता है लेखन सामग्री का अभाव रहा हो।
वैदिक शिक्षा में वैदिक मंत्रों की लिपि बध्यता धर्म के विपरीत थी, किंतु बौद्ध धर्म में तो लेखन कला सीखने की सहमति दी गई है तथा उसको जीविकोपार्जन का साधन बताया गया है।
केवल लेखन सामग्री की अप्राप्यता ही मौखिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन का मूल थी।
बौद्ध धर्म एक नवीन धर्म था। इसके प्रचार की आवश्यकता थी, और प्रचार की सफलता प्रचारक के ज्ञान और वाक् शक्ति पर निर्भर करती थी।
अतः बौद्ध शिक्षा में प्रश्नोत्तर, व्याख्यान एवं वाद-विवाद आदि का विशेष स्थान तथा ब्राह्मण सन्यासियों अथवा अन्य धर्म आचार्यों के सम्मुख में शास्त्रार्थ में विजयी होकर जन समुदाय को प्रभावित करने में समर्थ हो सके, इसलिए उच्च शिक्षा में वाद विवाद का निजी महत्त्व था।
विरोधियों के अतिरिक्त बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या के समाधान के लिए भी वाद-विवाद में पूर्णाभ्यस्त होना आवश्यक था।
विद्वत्सभा:-
नैतिकता को शिक्षा का अंग समझा जाता था।
बौद्ध धर्म में विद्वत्सभा का आयोजन नैतिक शिक्षा का एक माध्यम था,क्योंकि प्रतिमाह 2 बार विद्वत्सभा सभा का आयोजन कर विभिन्न संघों के विचारों को अपने अनैतिक कार्य सभा में उपस्थित करने पड़ते थे।
सभा में सभी भिक्षुओं का सम्मिलित होना अनिवार्य था।
कभी-कभी बीमार भिक्षुओं को भी उठाकर सभा के मध्य उपस्थित किया जाता था।
यदि वह इस योग्य भी ना हुआ तो सभा उसी के घर पर आयोजित की जाती थी, जिससे वह भी अपनी त्रुटियों को सबके समक्ष स्वीकार कर सके यदि की है तो, और सभा में उसकी उपस्थिति का भी प्रमाण रहे।
इन सभाओं का आयोजन पूर्णमासी और प्रतिपदा को किया जाता था।
यहां अधिकतर वैयक्तिक अपराधों पर विचार होता था। सामूहिक अपराध दूसरे क्षेत्र के विद्वानों के सामने रखे जाते थे।
इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष वार्षिक सभा का आयोजन किया जाता था जहां संघ को इस प्रकार की चुनौती सम्मानित व्यक्ति देते थे ,कि संघ उनको यदि दोषी या पवित्र सिद्ध कर सकता है तो करें।
इस प्रकार नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्वत्सभा का बड़ा महत्व था।
एकांत साधन:-
ब्राह्मण तपस्वियों के एकांत साधन, चिंतन और वास को बड़ा धार्मिक महत्व प्राप्त था।
बौद्ध भिक्षुओं को भी एकांत करते हुए,चिंतन और मनन में व्यस्त पाते हैं।
किंतु ब्राह्मण तपस्वियों और बौद्ध भिक्षुओं के एकांतवास में अंतर था।
बौद्ध भिक्षु प्रायः ऐसे स्थानों पर वास करते थे जहां से उनको भिक्षाटन के लिए दूर ना जाना पड़े तथा आने-जाने वाले भिक्षुओं की उचित सेवा करने में समर्थ हो सके।
ध्यान देने की बात यह है कि केवल वही भिक्षु निर्जन वन अथवा गुफाओं में निवास कर आध्यात्मिक चिंतन करते थे जिनको संघ के उत्तरदायित्व से शांति पाने की इच्छा होती, तथा सांसारिक माया-मोह का सर्वस्व लगाव छूट गया होता था।
बौद्ध कालीन जन सामान्य की शिक्षा:-
सामान्यतया बौद्ध संघ गृहस्थ जीवन त्याग कर आए हुए बौद्ध धर्मावलंबियों भिक्षुओं के लिए था।
संघ के यही स्थाई सदस्य होते थे और संघ इन्हीं की शिक्षा का प्रबंध करता था।
संघ में बौद्ध धर्म के गृहस्थ अनुयायियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।
किंतु अपने धर्म के मानने वालों को धार्मिक सिद्धांतों तथा अन्य आचरणों का ज्ञान कराना आवश्यक था ,और संघ भी अपने इस आवश्यक कर्तव्य के प्रति जागरूक था।
इसका एक कारण और भी था कि गृहस्थ बौद्ध धर्मावलंबियों के दान द्वारा ही संघ के बच्चों की दैनिक शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती थी।फिर इन ग्राहकों के प्रति संघ सर्वथा उदासीन कैसे रह सकता था।
इन ग्राहकों की शिक्षा देना और बौद्धों का कर्तव्य था और यह परिभ्रमण करते समय धार्मिक शिक्षा द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए धर्म के प्रति उनके मन में आस्था उत्पन्न करते थे।
ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के लिए अपने राज्य के 80 सहस्त्र ग्रामों के वासियों को आदेश दिया था।
किंतु इन ग्राहकों के बच्चों की मौलिक शिक्षा का कोई प्रबंध संघ की ओर से ना था।
संभवत बौद्ध धर्म के मानने वाले भी मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्कालीन अन्य शिक्षा संस्थाओं में जाते थे।
मिलिंद पन्ह के अनुसार ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा के विषय निम्नांकित थे।—-
बौद्ध कालीन शिक्षा के विषय:-
1.बौद्ध साहित्य धार्मिक।
2.विहारों के बनाने का क्रियात्मक ज्ञान।
3.विहारों को उपलब्ध दान- संपत्ति का लेखा रखने का ज्ञान आदि।
ब्राह्मण शिक्षा के विषय:-
चारों वेद, पुराण, इतिहास, व्याकरण, पद्य, ध्वनि, छंद, वेदांत,
जीवों की बोली, भूकंप, अपशकुन आदि का ज्ञान, सांख्य, न्याय योग,वैशेषिक संगीत, मंत्र, औषधि, युद्ध विद्या आदि।
वृहत शिक्षा संस्थाएं:-
भारत में कई शिक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर विदेशों से विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे
और उन शिक्षा केंद्रों में तक्षशिला का स्थान सर्वोच्च था जिसका प्रमुख कारण यह था कि तक्षशिला में आचार्य विख्यात विद्वान थे उनकी विद्वता सारे भारत में प्रसिद्ध थी।
उनको अपने विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान होता था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन भारत में तक्षशिला का शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व था।
विहार:-
बौद्ध शिक्षा पद्धति की मुख्य आधारशिला मठ अथवा विहार थी। विहारों में रहने वाले बच्चों की संघ से शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति होती थी।किसी किसी विहार अथवा मठ में 1000 तक भिक्षु रह सकते थे।
संघ के कुछ सामूहिक नियम होते थे जिनका पालन करते हुए आचार्य( उपाज्झयाय) अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पूरा करते थे।
नए भिक्षु अपने आचार्य (उपाज्झयाय) की संरक्षण में विद्या अध्ययन करते थे और आचार्य को प्रत्येक नवागंतुकों भिक्षुओं की शिक्षा का उत्तरदायित्व वाहन करना होता था।
इस प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में छोटे-छोटे विद्यालय एक सामूहिक समुदाय के अनुशासन में रहते थे।
छात्र इस बड़ी संख्या के सदस्य होते थे तथा उनके प्रत्येक व्यापार में उनको भाग लेने का अधिकार था।
कहा जा सकता है कि ब्राह्मण पद्धति के विपरीत बौद्ध शिक्षा पद्धति व्यक्ति होते हुए भी प्रणाली के अंतर्गत आती थी।
स्त्री शिक्षा:-
महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी थी
किंतु अपनी विमाता महा प्रजापति को जो कि बाद में 500 शाक्य क्षत्राणियों सहित संघ में प्रविष्ट हुई,
तथा अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह से बुध्द ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी।
स्त्रियों पर संघ के नियम आदि कठोर थे।
नव भिक्षुणी का परीक्षा काल 2 वर्ष का होता था। उनको भिक्षुओं से अलग रहना पड़ता था।
दैनिक जीवन भिक्षु और भिक्षुणियों का समान होने पर भी संघ में भिक्षुणियों का स्थान भिक्षुओं से नीचे समझा जाता था
और वह आचार्य के साथ अकेले नहीं रह सकती थी।
एक विशेष भिक्षु द्वारा मास में दो बार दूसरे भिक्षुओं की उपस्थिति में उन्हें शिक्षा तथा उपदेश देने की व्यवस्था थी।
किसी को भी स्थाई भिक्षु बनने के लिए संपूर्ण संघ की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
यह सब प्रतिबंध संघ में नारियों पर थे।
फिर भी भारतीय समाज में तथा बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों का महत्व स्पष्ट है।
भिक्षुणियों में अधिकतर धार्मिक प्रेरणा व संघ में सम्मिलित होने वाली महिलाएं थी।
किंतु कुछ भौतिक जगत के संकटों से उठकर शांति प्राप्त करने के निमित्त भिक्षुणी बन जाती थी।
इन दोनों प्रकार की भिक्षुणी महिलाओं में से कुछ तो अपनी विद्वता के लिए विख्यात थी।
सुखा का का नाम इस विषय में उल्लेखनीय है।
उसके प्रवचन द्वारा जन समुदाय अपने को कृत्य कृत्य करता था।
भिक्षुणियां शोक ग्रस्त महिलाओं के कष्ट निवारण के लिए तत्पर रहती थी।
पचारा नामक भिक्षुणी का नाम दयालु प्रवृत्ति के लिए सराहनीय है।
संघ के बाहर भी स्त्रियों में धर्म के प्रति बड़ी रूचि थी।
विशाखा, सूफिया, आम्रपाली आदि महिलाएं धर्म अनुरागी थी तथा उनकी दानशीलता का बौद्ध संघ बड़ा आभारी था।
व्यवसायिक शिक्षा:-
बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख आधार धर्म तथा और इस उद्देश्य की पूर्ति विहारों में होती थी।
किंतु उस समय औद्योगिक ज्ञान को भी उपेक्षित नहीं किया गया।
तत्कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था भिक्षुओं तक को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का ज्ञान इसलिए होना अनिवार्य था, जिससे कि वह अपने वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें।
विहारों के भवनों का उचित निर्माण करवाने के लिए उनको मकान बनाने की कला से भी परिचित होना आवश्यक था।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जीविकोपार्जन में सहायक उद्योगों की शिक्षा भी दी जाती थी।
बौद्ध कालीन औषधि:-
आयुर्वेद और शल्य विद्या उस समय अपनी बहुत उन्नति कर चुकी थी।
आयुर्वेद पिता चरक का प्रादुर्भाव उस काल में ही हुआ था।
राज परिचारिका सालवती का पुत्र “जीवक” उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सक था।
उसने तक्षशिला में किसी ख्याति प्राप्त औषधिवेत्ता का शिष्य रहकर 7 वर्ष तक औषधि विज्ञान का अध्ययन किया तत्पश्चात परीक्षा में सफलता प्राप्त कर गुरु का आशीर्वाद पाकर घर लौटा।
शिक्षा समाप्त करने के उपरांत जीवक ने विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण किया और रोगियों की चिकित्सा की।
अनेक असाध्य रोगों को उसने अच्छा किया।
जीवक द्वारा राजगृह की एक सेठ के मस्तिष्क को आधा काशी के एक अन्य पुत्र के पेट को चीरकर अच्छा किए जाने का वर्णन मिलता है।
अंग विशेष को चीरने के उपरांत जीवक मरहम लगाकर घाव को शीघ्र आराम पहुंचाता था।
जीवक के अतिरिक्त मिलिंदपन्हो में अन्य तत्कालीन औषधि वेत्ताओं का भी वर्णन विवरण मिलता है।
नारद, कपिल, अंगिरास, धनवंतरि और अतुल आदि प्रमुख चिकित्सा शास्त्री थे।
चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसके अंतर्गत ब्याधि की उत्पत्ति का कारण , उसका स्वभाव, उसकी चिकित्सा, उपचार की रीति, रोगी की परीक्षा संबंधी ज्ञान, किसी योग्य शिक्षक के द्वारा दी जाती थी।
शिक्षा शुल्क मुद्रा तथा परिश्रमिक रूप में चुकाना पड़ता था।
शल्य विद्या (ऑपरेशन) का विधिवत ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा का व्यवहारिक रूप भी प्रचलित था।
बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र
पाटलिपुत्र ,श्रावस्ती ,राजगृह,वैशाली,गया ,कुशीनगर,कान्यकुब्ज संकाश्य,काशी,चंपा,गांधार ,तक्षशिला ,सारनाथ ,
नालंदा कपिलवस्तु, मुंगेर, आनंदर, उदयन, मथुरा ,अयोध्या, मगध , विशोक, चीनभुक्ति,स्थानेश्वर, विशोक, चोला कांजीपुर तथा वल्लभी।
बौद्ध कालीन शिक्षा के विद्वान:-
महाकात्यायन, नागार्जुन, देव, वसुमित्र ,ईश्वर ,पार्षद, असंग, दिग्नाग,कुमारलब्धव, स्थिरमती ,नारायण देव ,
गुणप्रभु ,वसुबंधु गुणवती, धर्मपाल, जय गुप्त, मित्रसेन, चंद्र वर्मा ,प्राज्ञभद्र ,वीर्य सेन, शांति सेन ,तथागत गुप्त, पतंजलि, भर्तहरि आदि।
इस समय अनेक ग्रंथों की रचना हुई।
चीनी यात्री यहां से अनेक ग्रंथ अपने साथ स्वदेश ले गए
और उनका अनुवाद अपनी मातृभाषा में करके बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया।